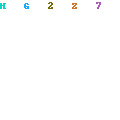बुधवार को हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों से हुई तबाही को गुरूवार की सुबह सुबह अखबारों में देख मन हिल गया। लाशों की तस्वीरें, घायलों के कराहते चेहरे, घटनास्थल पर पड़े चिथड़े दिनभर आंखों के सामने घूमते रहे। नेताओं के रुटीन, खोखले सांत्वना भरे बयानों की तरफ तो नज़र घुमाने की भी इच्छा न हुई। हर धमाके या आतंकी हमले के कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। अगले दिन शुक्रवार को अखबारों में पढ़ा- "फिर पटरी पर लौटी जिंदादिल मुंबई", "नए फौसले के साथ काम पर लौटे मुंबईवासी", "आतंक के मुंह पर तमाचा" जैसे शीर्षकों से अखबार सजे हुए थे। पढ़कर अच्छा लगा पर याद आया २००६ के हमलों के अगले दिन भी ऐसी ही खबरें अखबारों में छपी थी। मुंबई हो या कोई अन्य शहर जहां ऐसे हादसे हुए हों, वहां जिंदगी कुछ ही दिनों में पटरी पर आ जाती है। क्योंकि इस आपाधापी भरे जीवन में इंसान चाहकर भी नहीं रुक पाता। हां, लोगों में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है, वे उनका दर्द महसूस करते हैं। हमलावरों के साथ ही अशक्त सरकार के प्रति रोष भी है, कहीं डर भी है और साथ में है साहस आगे बढ़ने का। घायलों की स्थिति उन्हें द्रवित करती हैं। वे रुकना चाहते हैं पर जिंदगी की जिम्मेदारियां उनके कदम आगे ढकेल देती है। परंतु ऐसे हमलों के बाद नागरिकों द्वारा डर को पछाड़ते हुए जिंदादिली से आगे बढ़ना आतंक के मुंह पर तमाचा भी है। जनता अपने इस हौसले भरे कदम के साथ यह जताती है कि हम कमज़ोर नहीं। तुम आतंक फैला सकते हो पर हमारे हौसले के आगे ये बहुत छोटे हैं। इस तरह बुधवार के हमलों के बाद अगले दिन मुंबई का पटरी पर लौटना आतंकियों को करारा जवाब था।
अब प्रश्न उठता है कि सरकार कब इन हिसंक तत्वों के गाल पर तमाचा जडेगी। कब आतंकियों को ये संदेश देगी कि आइंदा हमला करने की योजना भी बनाई तो अपनी खैर मनाना। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी १३ जुलाई को हमले में मारे गए उन बेगुनाहों के परिवारवालों पर। उनके लिए तो जिंदगी मानो थम सी गई है। बाहर दुनिया चलायमान है, नेताओं की जुबानें चल रही हैं, आतंकियों की गोलियां चल रही हैं मगर उनके लिए जिंदगी उस एक पल में रुक गई है। जो घायल हुए हैं, उन पर क्या बीतती होगी जब वे टीवी पर घायलों को मुआवजे देने की खबर सुनते होंगे? क्या हमारे जान की कीमत चंद रुपये हैं। क्यों गया मैं उस जगह। काश घर में होता। क्या ऐसी कोई जगह है जहां मैं सुरिक्षत महसूस कर सकता हूं? कहीं इस अस्पताल में भी तो बम नहीं रखा है। ऐसे न जाने कितने प्रकार के सवाल बिस्तर पर लेटे उस घायल में मन में चलते होंगे। पर ये सवाल क्या सरकार चलाने वालों के मन में आते होंगे?
शायद नहीं। क्योंकि अगर आते होते तो ५ साल पहले मुंबई में खूनी खेल खेलने वाला कसाब अब तक जिंदा नहीं होता। अफजल गुरू जैसे दहशतगर्द को अब तक सजा मिल गई होती। इन हमलावरों को सजा न देकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि आइए हमला करिए और चैन से यहां रहिए। पांच साल पहले जब मुंबई हमला हुआ तब कहा गया कि चूक हुई है। चूक होना अलग बात है और उस चूक को न सुधारना दूसरी बात। हमले की वजह चूक थी पर कसाब को तत्काल फांसी देकर ये संदेश दिया जा सकता था कि हम पर हमला करने वाले का यही हश्र होता है। पर कसाब का अब तक जिंदा रहना ही आतंकियों के हौसले को बढ़ाने के लिए काफी है। मुंबई हमले २००६ में मारे गए लोगों के परिजन जब कसाब को जिंदा देखते होंगे, अखबारों में उस पर खर्च होती भारी मात्रा की खबर पढ़ते होंगे तो उनके दिल टूट जाते होंगे। लोकतंत्र और सरकार पर से तो उनका भरोसा उठ जाता होगा। आप ही बताइए क्या यही कसाब ९/११ के हमलों में अमेरिका में पकड़ा गया होता तो क्या वो अब तक जिंदा रहता। बिलकुल नहीं। उसे तो कबकी फांसी मिल चुकी होती।
फिर आखिर भारत आतंकवाद के मोर्चे पर कोई करारा जवाब देने से क्यों हिचकता है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मन को मारने की बात छोड़िए। अपने देश में खून की होली खेलने वाले हत्यारों को सजा देकर तो अपनी दृढ़ता दिखाई जा सकती है। अब तो बस आशा ही की जा सकती है कि कोई तो ठोस कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा। आतंकवाद का खात्मा कोई रातों रात या चंद दिनों में नहीं हो सकता। यह भी सत्य है कि कितनी भी चौकस व्यवस्था हो इतने बड़े देश के हर एक गली-मोहल्ले को सुरक्षित नहीं किया जा सकता किंतु आतंकवाद के खिलाफ छोटे-छोटे ठोस कदमों को बढ़ाकर पीड़ित जनता के घावों पर मरहम तो लगाया जा सकता है।
शुक्रवार, जुलाई 15, 2011 |
Category:
आलेख
|
1 comments